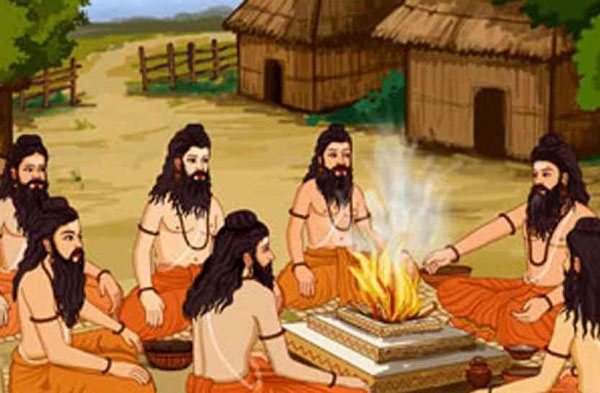ऋषि परम्परा से जुड़े होने का गौरव अनुभव करें, उसके जीवन्त अंग बनें
ऋषि पंचमी
ऋषि पंचमी का पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद (भादों) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाने का प्रचलन भारत में है। इस वर्ष यह पर्व १४ सितम्बर को पड़ रहा है। भारत की महानता के पीछे ऋषितंत्र की ही विशेष भूमिका रही है। पूरे भारत में हर वर्ग का गोत्र ऋषियों के नाम पर ही होता है। वंश या साधना- शोध प्रक्रिया के क्रम में जो वर्ग जिस ऋषि के निर्देशों- अनुशासनों का अनुपालन करता था, उसका गोत्र उसी ऋषि के नाम से ही बोला जाता रहा है। अर्थात् हर भारत वासी किसी न किसी रूप में ऋषि परम्परा के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। ऋषि परम्परा से जुड़े होने के नाते हर नर- नारी का पवित्र कर्त्तव्य बनता है कि वह अपने जीवन क्रम को ऋषि- अनुशासन के अनुरूप चलाता- विकसित करता रहे। इसी आत्म समीक्षा और आत्म शोधन- संवर्धन की प्रक्रिया को जीवन्त बनाये रखने के लिए ऋषि पंचमी का पर्व प्रतिष्ठित किया गया है।
आजकल तो इस पर्व का महत्त्व सामाजिक दृष्टि से बहुत कम रह गया है। कहीं- कहीं आस्थावान गृहणियाँ इस दिन चिह्न पूजा के रूप में उपवास एवं पर्व पूजन का कुछ क्रम चला लेती हैं। लेकिन व्रत रखने वाली देवियों सहित समाज के लोग इस पर्व के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को न समझते हैं और न अपनाते हैं। कथित ब्राह्मण और साधु वर्ग के व्यक्ति, जिनसे ऋषि अनुशासन निभाने और अन्य व्यक्तियों को भी उस दिश में प्रेरित करते रहने की आशा की जाती है, अधिकांश रूप में वे भी इस ओर उदासीन ही रहते हैं।
ऋषिगण जीवन जीने की कला जीवन- विज्ञान के सर्वोच्च विशेषज्ञ रहे हैं। आज व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में जो कष्टकारी- पतनोन्मुख विसंगतियाँ पनप रही हैं, उनमें से लगभग सभी ऋषियों द्वारा स्थापित जीवन- अनुशासन के उल्लंघन से उभरी हैं। उनका समाधान भी पुन: जनजीवन में ऋषि अनुशासनों की स्थापना से ही निकल सकता है। इसलिए ऋषि पंचमी पर्व के माध्यम से ऋषि गरिमा को समझने- समझाने, उनके जीवन सूत्रों को अपनाने, अभ्यास में लाने के प्रयास- प्रयोग किए जाने उचित भी हैं और आवश्यक भी। विशेष रूप से 'प्रज्ञा अभियान', युग निर्माण योजना से जुड़े परिजनों को तो इस दिशा में विशेष भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि युगऋषि ने मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य लाने, मनुष्य में देवत्व के जागरण और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए ऋषि परम्परा के पुनर्जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताई है। यह तथ्य जन- जन तक पहुँचाने के लिए ऋषि पंचमी को भी एक उपयुक्त माध्यम बनाया जा सकता है।
गौरवमय परम्परा
मनुष्यता के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो मनुष्य जीवन को गरिमामय बनाने में ऋषितंत्र की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दें :-
• सृष्टि के प्रारंभ में स्वायंभू (परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुए) मनु और शतरूपा ऋषिस्तर के ही थे। अवतारों में वामन, परशुराम, भगवान राम, कृष्ण आदि को काया रूप में लाने का आधार ऋषि स्तर के व्यक्तियों ने ही बनाया। वे ही परमात्म चेतना और मनुष्यों के बीच दिव्य सम्पर्क सूत्र बने रहे।
• अवतारी पुरुषों को निखारने- उभारने की अद्भुत प्रक्रिया अपने- अपने समय के ऋषिकल्प व्यक्तियों ने ही चलायी।
• ज्ञान- विज्ञान, कला- संस्कृति के विकास के लिए शोध- तप, प्रयोग, प्रसार, प्रशिक्षण की व्यवस्थित प्रक्रियाएँ उन्हीं ने चलायीं। ज्ञान के प्रथम और सर्वोच्च माने जाने वाले संस्करण, वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण एवं आरण्यक सूत्रों की रचना, संकलन- सम्पादन की जिम्मेदारी भी ऋषितंत्र ने निभायी।
• योग- विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिर्विज्ञान, संगीत, चिकित्सा विज्ञान आदि की विभिन्न धाराएँ भी ऋषि परम्परा की प्रतिभाओं ने ही अवतरित, विकसित एवं प्रसारित कीं। पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान और चेतना विज्ञान (अध्यात्म) को विकसित और परस्पर पूरक बनाने वाले भी वही रहे।
• विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की भिन्नताओं के बीच विकसित विविध सांस्कृतिक धाराओं से जुड़े, विभिन्न धर्म- आस्था वाले व्यक्तियों के बीच 'वसुधैव कुटुम्बकम', 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दिव्य अनुभूति के आधार पर अनेकता में एकता का बोध उन्हीं ने किया और कराया।
• धर्म विज्ञान के मूल आध्यात्मिक सूत्रों के साथ क्षेत्र और समय विशेष की आवश्यकताओं की संगति बिठाते हुए ईश्वरीय संदेशों को जन- जन तक पहुँचाने वाले, उनके अनुपालन हेतु मार्गदर्शन और शक्ति अनुदान देने वाले, विभिन्न धर्म- सम्प्रदायों के प्रणेता सभी ऋषि परम्परा के ही महापुरुष थे।
इन सूत्रों पर प्रकाश डालने का मूल प्रयोजन यही है कि जन- जन का ध्यान ऋषि परम्परा के गरिमामय स्वरूप और उनके सम्बन्ध, अनुशासनों की आवश्यकता की ओर लाया जाय तो मनुष्य के चिन्तन, चरित्र और व्यवहार में आये भटकाव एवं उस कारण उपजी अनेक कठिनाइयों का उपचार किया जा सकता है। मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य का पुष्ट आधार तैयार किया जा सकता है।
सत्य यह नहीं है कि समय के साथ उभरे विज्ञान युग के शोध प्रयोगों ने मनुष्य के लिए जो सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं, शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, उनके कारण मनुष्य के जीवन में भटकाव आ गया है। सत्य यह है कि भौतिक शक्तियों- सुविधाओं के सदुपयोग की दिशा- प्रेरणा देने में समर्थ ऋषि सूत्रों को भुला देने के कारण मनुष्य समाज भटक कर विकास के भ्रम में विनाश के सरंजाम जुटाने लगा है।
युगऋषि के समाधान
युगऋषि (वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा) ने इस दिशा में बहुत विवेकसम्मत और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। जैसे :-
लौकिक शक्तियाँ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होतीं। उनका सदुपयोग या दुरुपयोग ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। जितनी समर्थ शक्ति हो, उसे नियंत्रित करके सही दिशा में, सही प्रयोजनों में लगा देने के लिए उसी स्तर की आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में ही लौकिक शक्तियाँ अनियंत्रित होकर अर्थ का अनर्थ करने लगती हैं। उदाहरण देखें :-
सैन्य शक्ति : इसे बढ़ाने का मूल प्रयोजन जन- जन को सुरक्षा प्रदान करना है। इस शक्ति का खूब विकास हुआ है। शरीर की शक्ति से प्रारम्भ होकर अस्त्र- शस्त्रों, तीर- तलवारों, बन्दूकों- तोपों से होते हुए परमाणु बम तक इसका विकास हो गया है। लेकिन कोई भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। इसकी दिशा बहक जाने से यह गुण्डागर्दी, उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
अर्थशक्ति : इसकी आवश्यकता जन- जन को पोषण- आरोग्य, दीर्घ जीवन प्रदान करने के लिए है। अनुशासनहीन होकर यही शोषण, व्यसन, रोग आदि को बढ़ावा दे रही है। लोग अज्ञानग्रस्त होकर इस साधन को ही साध्य मानने लगे हैं। इसे पाने के नशे में लोग मनुष्यता को भूलकर पशु और पिशाच स्तर तक गिर जाते हैं।
बुद्धिशक्ति : इसकी आवश्यकता मनुष्य को विभिन्न विषयों में कुशल और विवेकशील बनाने के लिए है। लेकिन यह भटक कर छल, प्रपंच, पाखंड और घोटाले बढ़ाने में लग रही है। समाज को पीड़ित- प्रताड़ित करने वाली दुष्प्रवृत्तियों को बुद्धि से कमजोर व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। दुर्बुद्धि से दुरुपयोग और दुरुपयोग से दुर्गति की उक्ति सर्वमान्य है। ऋषि प्रणीत सूत्रों के अनुसरण से उक्त तीनों शक्तियों को सद्बुद्धि से सदुपयोग और सदुपयोग से सद्गति के कल्याणकारी मार्ग पर लाया जा सकता है।
लोग अपनी ऋषि परम्परा, उससे प्राप्त शानदार विरासत को भूल गये हैं। वे अपने आप को इस समय की विकृत परम्पराओं का ही अंग मानने लगे हैं। चेतन होते हुए भी जड़- निर्जीव पदार्थों की तरह जमाने की धारा में बहते जाना ही अपनी नियति मान बैठे हैं। हम समाज को उत्कर्ष की दिशा और शक्ति देने वाले ऋषियों की गौरवमयी परम्परा के अंग हैं, यह भाव जागते ही परिदृश्य बदलने लगेगा। बेजान तिनकों, पत्तों, लकड़ी के टुकड़ों की तरह धारा में बहने वाले व्यक्ति चेतना सम्पन्न जल जीवों की तरह धाराओं को चीरते हुए अपने- अपने गरिमामय लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगेंगे।
समझें- समझायें, बढ़ें- बढ़ायें
युगऋषि से गहन आस्था के साथ जुड़े हुए उनके शिष्य, अनुयायी अंग- अवयव कहलाने वाले प्रजा परिजनों, प्रज्ञापुत्र- पुत्रियों को ऋषि सूत्रों को समझने- समझाने, उस दिशा में बढ़ने- बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार और सक्रिय करना ही चाहिए। इसी आधार पर वे युग परिवर्तन के ईश्वरीय अभियान में अग्रदूतों की सफल भूमिका निभा सकते हैं। युगधर्म का कुशल निर्वाह करते हुए उच्चस्तरीय श्रेय- सुयश और सद्गति के अधिकारी बन सकते हैं।
ध्यान रहे इसके लिए ऋषि सूत्रों को रट लेना और लोगों से दुहरवा लेना भर काफ़ी नहीं है। गीता पढ़ी और रटी तो बहुतों ने है, किन्तु स्थितप्रज्ञ बनने की दिशा में, अपनी संकीर्णता को विसर्जित करके प्रभु की विराटता की अनुभूति करने में कितने सफल हुए?
पतंजलि के योग सूत्र पढ़ना, याद करना तो किसी के लिए संभव है, किन्तु क्या इतने मात्र से वे योग सिद्ध साधक बन सकते हैं?
वेदान्त के सूत्र बहुतों को याद हैं, किन्तु इतने भर से क्या वे सारे विश्व के साथ एकात्मता का बोध कर सकते हैं?
युगऋषि ने कहा है कि यह सब पहले चरण के रूप में ठीक हो सकते हैं, किन्तु अगले चरणों की सिद्धि के लिए साधकों को अपने प्राणों को, व्यक्तित्व को उसके अनुरूप परिष्कृत- विकसित करना पड़ता है। उन्होंने लिखा है:-
अध्यापक बहुत होते हैं, पर जो अपनी प्राण चेतना से, संपर्क में आने वालों का प्राण उपचार कर सकें, ऐसे ऋषिकल्प देवमानव कम ही होते हैं। जो होते हैं वे ज्ञान के साथ- साथ सदा उत्कृष्टता का अमृत पिलाते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं और जीवन की दिशाधारा में उच्च स्तरीय महान परिवर्तन करते हैं। (प्रज्ञोपनिषद् ६/२/८०- ८३)
इस प्रकार वाँछित दिशा में श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए केवल आत्मकल्याण की साधना ही पर्याप्त नहीं होती, उनके साथ लोकमंगल की साधना का भी संतुलित क्रम चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रणाली पर प्रकाश डलते हुए वे लिखते हैं:-
इसके लिए व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने के उपरान्त वे (ऋषितंत्र के व्यक्ति) इस संचित विभूति के आधार पर अपने उदार पुरुषार्थ का उपयोग जन- जन का आन्तरिक परिष्कार करने में लगाते हैं। यही सनातन ऋषि धर्म है। इसी प्रयोजन के लिए वे समयासनुसार अनेक योजनाएँ बनाते और कार्यक्रम चलाते रहते हैं। (प्रज्ञो. ६/२/ ८४- ८६)
प्रज्ञा परिजन इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए युगऋषि के दिए हुए जीवन साधना सूत्रों से व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हुए जनमानस के परिष्कार को अपनी साधना की कसौटी मानकर लग पड़ें तो काम बनने लगे। इससे अपनी क्षमता बढ़ने या सफलता मिलने का अहंकार नहीं पनपेगा और आत्म संतोष, लोकसम्मान तथा दैवी अनुग्रह की बढ़तोत्तरी का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
जिनमें मानसिक परिष्कार के प्रति उत्साह दिखाई दे, उन्हें तत्काल किसी सुगम- सुनियोजित कार्यक्रम में लगा दिया जाय। पू. गुरुदेव ने युग सैनिकों के लिए आत्मकल्याण और लोकमंगल की साधनाओं के साथ ऋषिधर्म- युगधर्म निभाने के लिए समुचित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रारूप भी बना दिए हैं। उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर निष्ठापूर्वक चलने वालों के साथ उनकी शक्तिधाराएँ भी जुड़ जाती हैं, इस तथ्य की अनुभूति भी हममें से लगभग सभी को है। उनके निर्धारित क्रम का अनुपालन करते हुए हम भी नवयुग, प्रज्ञायुग के लिए अनुकुल प्राणवान वातावरण बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है:-
पुरातन काल का सतयुग और कुछ नहीं, केवल मुनि- मनीषियों द्वारा उत्पन्न किए और बिखेरे गए सद्ज्ञान का ही प्रतिफल था। (प्रज्ञोपनिषद ६/२/८९)
प्राचीन काल में सतयुग के लिए ऋषियों ने उस समय के अनुरूप व्यवस्था बनायी होगी। वर्तमान काल में युग परिवर्तन में सक्षम सद्ज्ञान को उत्पन्न- विकसित करने का कठिन कार्य युगऋषि ने स्वयं कर दिया है। युग सैनिकों के हिस्से में उन्हें उर्वर भूमि पर बिखेरने की भूमिका आयी है। इतना होने पर उन बीजों को विकसित, पल्लवित, पुष्पित, फलित करने का कार्य महाकाल की युगान्तरीय चेतना कर देगी।
अस्तु ऋषि पंचमी पर सभी परिजनों को चाहिए कि वे अपने जीवन की गहन समीक्षा करें और ऋषि अनुशासन के अनुरूप अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को श्रेष्ठतर स्तर पर ले जाने की ठानें। अपने प्रभावक्षेत्र के व्यक्तियों को भी इस हेतु प्रेरित करें। इस दिशा में परस्पर एक- दूसरे को सहयोग देते रहने का क्रम बनाएँ। ऐसा करके हम सब ऋषि चरणों में सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे।
ऋषि पंचमी
ऋषि पंचमी का पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद (भादों) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाने का प्रचलन भारत में है। इस वर्ष यह पर्व १४ सितम्बर को पड़ रहा है। भारत की महानता के पीछे ऋषितंत्र की ही विशेष भूमिका रही है। पूरे भारत में हर वर्ग का गोत्र ऋषियों के नाम पर ही होता है। वंश या साधना- शोध प्रक्रिया के क्रम में जो वर्ग जिस ऋषि के निर्देशों- अनुशासनों का अनुपालन करता था, उसका गोत्र उसी ऋषि के नाम से ही बोला जाता रहा है। अर्थात् हर भारत वासी किसी न किसी रूप में ऋषि परम्परा के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। ऋषि परम्परा से जुड़े होने के नाते हर नर- नारी का पवित्र कर्त्तव्य बनता है कि वह अपने जीवन क्रम को ऋषि- अनुशासन के अनुरूप चलाता- विकसित करता रहे। इसी आत्म समीक्षा और आत्म शोधन- संवर्धन की प्रक्रिया को जीवन्त बनाये रखने के लिए ऋषि पंचमी का पर्व प्रतिष्ठित किया गया है।
आजकल तो इस पर्व का महत्त्व सामाजिक दृष्टि से बहुत कम रह गया है। कहीं- कहीं आस्थावान गृहणियाँ इस दिन चिह्न पूजा के रूप में उपवास एवं पर्व पूजन का कुछ क्रम चला लेती हैं। लेकिन व्रत रखने वाली देवियों सहित समाज के लोग इस पर्व के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को न समझते हैं और न अपनाते हैं। कथित ब्राह्मण और साधु वर्ग के व्यक्ति, जिनसे ऋषि अनुशासन निभाने और अन्य व्यक्तियों को भी उस दिश में प्रेरित करते रहने की आशा की जाती है, अधिकांश रूप में वे भी इस ओर उदासीन ही रहते हैं।
ऋषिगण जीवन जीने की कला जीवन- विज्ञान के सर्वोच्च विशेषज्ञ रहे हैं। आज व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में जो कष्टकारी- पतनोन्मुख विसंगतियाँ पनप रही हैं, उनमें से लगभग सभी ऋषियों द्वारा स्थापित जीवन- अनुशासन के उल्लंघन से उभरी हैं। उनका समाधान भी पुन: जनजीवन में ऋषि अनुशासनों की स्थापना से ही निकल सकता है। इसलिए ऋषि पंचमी पर्व के माध्यम से ऋषि गरिमा को समझने- समझाने, उनके जीवन सूत्रों को अपनाने, अभ्यास में लाने के प्रयास- प्रयोग किए जाने उचित भी हैं और आवश्यक भी। विशेष रूप से 'प्रज्ञा अभियान', युग निर्माण योजना से जुड़े परिजनों को तो इस दिशा में विशेष भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि युगऋषि ने मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य लाने, मनुष्य में देवत्व के जागरण और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए ऋषि परम्परा के पुनर्जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताई है। यह तथ्य जन- जन तक पहुँचाने के लिए ऋषि पंचमी को भी एक उपयुक्त माध्यम बनाया जा सकता है।
गौरवमय परम्परा
मनुष्यता के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो मनुष्य जीवन को गरिमामय बनाने में ऋषितंत्र की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दें :-
• सृष्टि के प्रारंभ में स्वायंभू (परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुए) मनु और शतरूपा ऋषिस्तर के ही थे। अवतारों में वामन, परशुराम, भगवान राम, कृष्ण आदि को काया रूप में लाने का आधार ऋषि स्तर के व्यक्तियों ने ही बनाया। वे ही परमात्म चेतना और मनुष्यों के बीच दिव्य सम्पर्क सूत्र बने रहे।
• अवतारी पुरुषों को निखारने- उभारने की अद्भुत प्रक्रिया अपने- अपने समय के ऋषिकल्प व्यक्तियों ने ही चलायी।
• ज्ञान- विज्ञान, कला- संस्कृति के विकास के लिए शोध- तप, प्रयोग, प्रसार, प्रशिक्षण की व्यवस्थित प्रक्रियाएँ उन्हीं ने चलायीं। ज्ञान के प्रथम और सर्वोच्च माने जाने वाले संस्करण, वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण एवं आरण्यक सूत्रों की रचना, संकलन- सम्पादन की जिम्मेदारी भी ऋषितंत्र ने निभायी।
• योग- विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिर्विज्ञान, संगीत, चिकित्सा विज्ञान आदि की विभिन्न धाराएँ भी ऋषि परम्परा की प्रतिभाओं ने ही अवतरित, विकसित एवं प्रसारित कीं। पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान और चेतना विज्ञान (अध्यात्म) को विकसित और परस्पर पूरक बनाने वाले भी वही रहे।
• विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की भिन्नताओं के बीच विकसित विविध सांस्कृतिक धाराओं से जुड़े, विभिन्न धर्म- आस्था वाले व्यक्तियों के बीच 'वसुधैव कुटुम्बकम', 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दिव्य अनुभूति के आधार पर अनेकता में एकता का बोध उन्हीं ने किया और कराया।
• धर्म विज्ञान के मूल आध्यात्मिक सूत्रों के साथ क्षेत्र और समय विशेष की आवश्यकताओं की संगति बिठाते हुए ईश्वरीय संदेशों को जन- जन तक पहुँचाने वाले, उनके अनुपालन हेतु मार्गदर्शन और शक्ति अनुदान देने वाले, विभिन्न धर्म- सम्प्रदायों के प्रणेता सभी ऋषि परम्परा के ही महापुरुष थे।
इन सूत्रों पर प्रकाश डालने का मूल प्रयोजन यही है कि जन- जन का ध्यान ऋषि परम्परा के गरिमामय स्वरूप और उनके सम्बन्ध, अनुशासनों की आवश्यकता की ओर लाया जाय तो मनुष्य के चिन्तन, चरित्र और व्यवहार में आये भटकाव एवं उस कारण उपजी अनेक कठिनाइयों का उपचार किया जा सकता है। मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य का पुष्ट आधार तैयार किया जा सकता है।
सत्य यह नहीं है कि समय के साथ उभरे विज्ञान युग के शोध प्रयोगों ने मनुष्य के लिए जो सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं, शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, उनके कारण मनुष्य के जीवन में भटकाव आ गया है। सत्य यह है कि भौतिक शक्तियों- सुविधाओं के सदुपयोग की दिशा- प्रेरणा देने में समर्थ ऋषि सूत्रों को भुला देने के कारण मनुष्य समाज भटक कर विकास के भ्रम में विनाश के सरंजाम जुटाने लगा है।
युगऋषि के समाधान
युगऋषि (वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा) ने इस दिशा में बहुत विवेकसम्मत और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। जैसे :-
लौकिक शक्तियाँ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होतीं। उनका सदुपयोग या दुरुपयोग ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। जितनी समर्थ शक्ति हो, उसे नियंत्रित करके सही दिशा में, सही प्रयोजनों में लगा देने के लिए उसी स्तर की आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में ही लौकिक शक्तियाँ अनियंत्रित होकर अर्थ का अनर्थ करने लगती हैं। उदाहरण देखें :-
सैन्य शक्ति : इसे बढ़ाने का मूल प्रयोजन जन- जन को सुरक्षा प्रदान करना है। इस शक्ति का खूब विकास हुआ है। शरीर की शक्ति से प्रारम्भ होकर अस्त्र- शस्त्रों, तीर- तलवारों, बन्दूकों- तोपों से होते हुए परमाणु बम तक इसका विकास हो गया है। लेकिन कोई भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। इसकी दिशा बहक जाने से यह गुण्डागर्दी, उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
अर्थशक्ति : इसकी आवश्यकता जन- जन को पोषण- आरोग्य, दीर्घ जीवन प्रदान करने के लिए है। अनुशासनहीन होकर यही शोषण, व्यसन, रोग आदि को बढ़ावा दे रही है। लोग अज्ञानग्रस्त होकर इस साधन को ही साध्य मानने लगे हैं। इसे पाने के नशे में लोग मनुष्यता को भूलकर पशु और पिशाच स्तर तक गिर जाते हैं।
बुद्धिशक्ति : इसकी आवश्यकता मनुष्य को विभिन्न विषयों में कुशल और विवेकशील बनाने के लिए है। लेकिन यह भटक कर छल, प्रपंच, पाखंड और घोटाले बढ़ाने में लग रही है। समाज को पीड़ित- प्रताड़ित करने वाली दुष्प्रवृत्तियों को बुद्धि से कमजोर व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। दुर्बुद्धि से दुरुपयोग और दुरुपयोग से दुर्गति की उक्ति सर्वमान्य है। ऋषि प्रणीत सूत्रों के अनुसरण से उक्त तीनों शक्तियों को सद्बुद्धि से सदुपयोग और सदुपयोग से सद्गति के कल्याणकारी मार्ग पर लाया जा सकता है।
लोग अपनी ऋषि परम्परा, उससे प्राप्त शानदार विरासत को भूल गये हैं। वे अपने आप को इस समय की विकृत परम्पराओं का ही अंग मानने लगे हैं। चेतन होते हुए भी जड़- निर्जीव पदार्थों की तरह जमाने की धारा में बहते जाना ही अपनी नियति मान बैठे हैं। हम समाज को उत्कर्ष की दिशा और शक्ति देने वाले ऋषियों की गौरवमयी परम्परा के अंग हैं, यह भाव जागते ही परिदृश्य बदलने लगेगा। बेजान तिनकों, पत्तों, लकड़ी के टुकड़ों की तरह धारा में बहने वाले व्यक्ति चेतना सम्पन्न जल जीवों की तरह धाराओं को चीरते हुए अपने- अपने गरिमामय लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगेंगे।
समझें- समझायें, बढ़ें- बढ़ायें
युगऋषि से गहन आस्था के साथ जुड़े हुए उनके शिष्य, अनुयायी अंग- अवयव कहलाने वाले प्रजा परिजनों, प्रज्ञापुत्र- पुत्रियों को ऋषि सूत्रों को समझने- समझाने, उस दिशा में बढ़ने- बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार और सक्रिय करना ही चाहिए। इसी आधार पर वे युग परिवर्तन के ईश्वरीय अभियान में अग्रदूतों की सफल भूमिका निभा सकते हैं। युगधर्म का कुशल निर्वाह करते हुए उच्चस्तरीय श्रेय- सुयश और सद्गति के अधिकारी बन सकते हैं।
ध्यान रहे इसके लिए ऋषि सूत्रों को रट लेना और लोगों से दुहरवा लेना भर काफ़ी नहीं है। गीता पढ़ी और रटी तो बहुतों ने है, किन्तु स्थितप्रज्ञ बनने की दिशा में, अपनी संकीर्णता को विसर्जित करके प्रभु की विराटता की अनुभूति करने में कितने सफल हुए?
पतंजलि के योग सूत्र पढ़ना, याद करना तो किसी के लिए संभव है, किन्तु क्या इतने मात्र से वे योग सिद्ध साधक बन सकते हैं?
वेदान्त के सूत्र बहुतों को याद हैं, किन्तु इतने भर से क्या वे सारे विश्व के साथ एकात्मता का बोध कर सकते हैं?
युगऋषि ने कहा है कि यह सब पहले चरण के रूप में ठीक हो सकते हैं, किन्तु अगले चरणों की सिद्धि के लिए साधकों को अपने प्राणों को, व्यक्तित्व को उसके अनुरूप परिष्कृत- विकसित करना पड़ता है। उन्होंने लिखा है:-
अध्यापक बहुत होते हैं, पर जो अपनी प्राण चेतना से, संपर्क में आने वालों का प्राण उपचार कर सकें, ऐसे ऋषिकल्प देवमानव कम ही होते हैं। जो होते हैं वे ज्ञान के साथ- साथ सदा उत्कृष्टता का अमृत पिलाते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं और जीवन की दिशाधारा में उच्च स्तरीय महान परिवर्तन करते हैं। (प्रज्ञोपनिषद् ६/२/८०- ८३)
इस प्रकार वाँछित दिशा में श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए केवल आत्मकल्याण की साधना ही पर्याप्त नहीं होती, उनके साथ लोकमंगल की साधना का भी संतुलित क्रम चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रणाली पर प्रकाश डलते हुए वे लिखते हैं:-
इसके लिए व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने के उपरान्त वे (ऋषितंत्र के व्यक्ति) इस संचित विभूति के आधार पर अपने उदार पुरुषार्थ का उपयोग जन- जन का आन्तरिक परिष्कार करने में लगाते हैं। यही सनातन ऋषि धर्म है। इसी प्रयोजन के लिए वे समयासनुसार अनेक योजनाएँ बनाते और कार्यक्रम चलाते रहते हैं। (प्रज्ञो. ६/२/ ८४- ८६)
प्रज्ञा परिजन इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए युगऋषि के दिए हुए जीवन साधना सूत्रों से व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हुए जनमानस के परिष्कार को अपनी साधना की कसौटी मानकर लग पड़ें तो काम बनने लगे। इससे अपनी क्षमता बढ़ने या सफलता मिलने का अहंकार नहीं पनपेगा और आत्म संतोष, लोकसम्मान तथा दैवी अनुग्रह की बढ़तोत्तरी का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
जिनमें मानसिक परिष्कार के प्रति उत्साह दिखाई दे, उन्हें तत्काल किसी सुगम- सुनियोजित कार्यक्रम में लगा दिया जाय। पू. गुरुदेव ने युग सैनिकों के लिए आत्मकल्याण और लोकमंगल की साधनाओं के साथ ऋषिधर्म- युगधर्म निभाने के लिए समुचित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रारूप भी बना दिए हैं। उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर निष्ठापूर्वक चलने वालों के साथ उनकी शक्तिधाराएँ भी जुड़ जाती हैं, इस तथ्य की अनुभूति भी हममें से लगभग सभी को है। उनके निर्धारित क्रम का अनुपालन करते हुए हम भी नवयुग, प्रज्ञायुग के लिए अनुकुल प्राणवान वातावरण बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है:-
पुरातन काल का सतयुग और कुछ नहीं, केवल मुनि- मनीषियों द्वारा उत्पन्न किए और बिखेरे गए सद्ज्ञान का ही प्रतिफल था। (प्रज्ञोपनिषद ६/२/८९)
प्राचीन काल में सतयुग के लिए ऋषियों ने उस समय के अनुरूप व्यवस्था बनायी होगी। वर्तमान काल में युग परिवर्तन में सक्षम सद्ज्ञान को उत्पन्न- विकसित करने का कठिन कार्य युगऋषि ने स्वयं कर दिया है। युग सैनिकों के हिस्से में उन्हें उर्वर भूमि पर बिखेरने की भूमिका आयी है। इतना होने पर उन बीजों को विकसित, पल्लवित, पुष्पित, फलित करने का कार्य महाकाल की युगान्तरीय चेतना कर देगी।
अस्तु ऋषि पंचमी पर सभी परिजनों को चाहिए कि वे अपने जीवन की गहन समीक्षा करें और ऋषि अनुशासन के अनुरूप अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को श्रेष्ठतर स्तर पर ले जाने की ठानें। अपने प्रभावक्षेत्र के व्यक्तियों को भी इस हेतु प्रेरित करें। इस दिशा में परस्पर एक- दूसरे को सहयोग देते रहने का क्रम बनाएँ। ऐसा करके हम सब ऋषि चरणों में सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे।