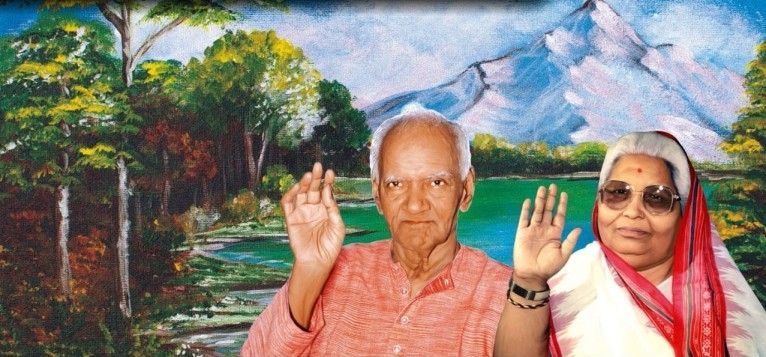युगऋषि के निर्देशानुसार 'ब्राह्मण मन' विकसित करने की ठानें
महापर्व- श्रावणी पर्व
श्रावणी पर्व का महत्त्व ऋषि परम्परा के अनुसार बहुत अधिक रहा है। यह पर्व द्विजत्व को विकसित और पुष्ट बनाने वाला विशिष्ट पर्व रहा है। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर दिव्य क्षमताएँ बीज रूप में होती हैं। उन्हें संतुलित साधना द्वारा विकसित करके हर व्यक्ति मानव से महामानव- देवमानव बन सकता है। नर से नारायण बनने के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ऋषिकल्प- गुरुओं के अनुशासन में उस संतुलित साधना को अपनाने के संकल्पयुक्त संस्कार को द्विजत्व का संस्कार कहा जाता है। मनुष्य उसी काया के रहते नये जन्म, दूसरे दिव्य जन्म का लाभ उठा सकता है। इस संस्कार के द्वारा ऋषि अनुग्रह और अपने साधना पुरुषार्थ के सुसंयोग से साधक अपने व्यक्तित्व में नयी सृष्टि का अनुपम लाभ प्राप्त करता है। युगऋषि ने पर्वों के महत्त्व के क्रम में यह लिखा है कि श्रावणी पर्व का सम्बन्ध उस समय से है, जब परब्रह्म- परमात्मा ने 'एकोऽहम बहुस्याम' का संकल्प किया। परब्रह्म का संकल्प होते ही उनकी अभिन्न चेतन शक्ति- आद्यशक्ति ने तत्काल सृष्टि को स्वरूप प्रदान कर दिया। इस नाते श्रावणी पर्व के साथ आदिशक्ति- चिद्शक्ति का सृजनशील प्रवाह जुड़ा रहता है। साधक के अन्दर कोई सत्संकल्प आकार लेता है तो वह शक्ति उसे साकार करने के लिए अपना समर्थ सहयोग अनायास ही प्रदान करने लगती है। साधक इस दिव्य ऊर्जा प्रवाह का लाभ उठाकर अपने जीवन में एक नयी सृष्टि करने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए इसे द्विजत्व के संकल्प को परिष्कृत और पुष्ट बनाकर जीवन लक्ष्य तक पहुँचने के पुण्य पर्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।
संकल्प कैसा : प्रश्न है कि जब प्रकृति का प्रवाह श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने की दिव्य ऊर्जा के साथ अवतरित हो रहा हो तो कैसा संकल्प किया जाय? चिन्तन करने पर सहज ही यह उत्तर उभरेगा कि ऐसे मौके पर सोने जैसा खरा और बड़ा संकल्प लिया जाय। इसीलिए ऋषियों ने श्रावणी पर्व के संकल्प को हेमाद्रि संकल्प नाम दिया। हेम शुद्ध सोने को कहते हैं और अद्रि पर्वत का पर्याय है। अर्थात् ऐसे महत्त्वपूर्ण पर्व पर शुद्ध सोने के पर्वत जैसा संकल्प करना चाहिए। जीवन को द्विजत्व के मार्ग से नर से नारायण के स्तर पर ले जाने वाले संकल्प को ही वास्तव में हेमाद्रि संकल्प कहा जा सकता है।
श्रावणी पर्व पर हेमाद्रि संकल्प के साथ जुड़े अन्य कर्मकाण्ड दश स्नान, ऋषि पूजन, वेद पूजन आदि भी द्विजत्व की साधना को सिद्ध करने के सूत्रों को हृदयंगम कराने वाले हैं। आवश्यकता है उन्हें यंत्रवत पूरा न करके उनके अनुरूप भावनाओं को जाग्रत् और सक्रिय किया जाय। इसी आधार पर विकसित की गयी साधना वे परिणाम उत्पन्न करती है, जिन्हें ऋषियों- मनीषियों ने अद्भुत- अनुपम कहा है।
ऋषियुग्म के अनुभव अपनी जीवनी 'हमारी वसीयत और विरासत' में युगऋषि ने साधना के कर्मकाण्डों से अधिक महत्त्व उनसे सम्बद्ध भावनाओं को देने की बात कही है। अपनी सफल साधना का मर्म समझाते हुए वे लिखते हैं-
"हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। निर्धारित जप संख्या को पूरा करने का अनुशासन कठोरतापूर्वक पाला गया। आपात स्थिति में कोई कमी रह गयी तो उसे अगले दिनों में पूरा कर लिया गया। इसी के साथ उस अवधि में भावनाओं से ओतप्रोत रहने कीमनःस्थिति बनाये रहने का अभ्यास किया गया है और वह सफल भी होता रहा है। समर्पण, एकता, एकात्मता, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ में कल्पना के रूप में किया गया था। पीछे वह मान्यता बन गयी और अन्त में अनुभूति प्रतीत होने लगी।"
संकल्पित जप- कर्मकाण्ड आदि का पालन पूरी निष्ठा से करने के साथ ही साथ इष्ट के अनुकूल भावनाओं को जीवन्त और सतत बनाये रखने के प्रयास भी पूरी तत्परता से करने के संकल्पित प्रयासों ने उनकी साधना को सिद्धि तक पहुँचाया। इस प्रयास में भी कई साधक बीच में ही उलझकर रह जाते हैं। कल्पना को ही उपलब्धि मानकर आत्मसम्मोहन की स्थिति में ही जीते रहते हैं, मान्यता और अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच पाते। इस सम्मोहन से उबरने के लिए बहुत विवेकपूर्वक ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण- परीक्षण भी करना पड़ता है। गुरुवर ने इस सम्बन्ध में लिखा है :-
'गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी। यह मात्र कल्पना तो नहीं है, इसके लिए बार- बार कठोर आत्म निरीक्षण किया जाता रहा। देखा गया कि आदर्श जीवन के प्रति- समष्टि के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं? आदर्शों के लिए प्रलोभनों और दबावों से इन्कार करने की स्थिति है या नहीं? समय- समय पर घटनाओं से जोड़कर भी परख की गयी और पाया गया कि भावना परिपक्व हो गयी है। ... मान्यता का गुण- कर्म में परिवर्तन होना, यही तो उपासनात्मक धारणा की परख है।'
बालक श्रीराम को उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय यह बात समझाई गयी थी कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। उन्होंने अपने मन- अन्तःकरण को ब्राह्मण के स्तर का बनाने की भावभरी तप साधना की। उन्हें उसका भरपूर लाभ मिला। उन्हीं के चरण- चिह्नों पर चलते हुए हम सबकों 'ब्राह्मणत्व संवर्धन' के पर्व श्रावणी पर अपने मन को ब्राह्मण के साँचे में ढालने के प्रयास किये जाने चाहिये। अपने साधना पुरुषार्थके लाभ उन्हीं की तरह कमाने की भूमिका बनानी चाहिये।
ब्राह्मणत्व का महत्त्व
समय- समय पर ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर आते हैं, जिनका लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति प्रचुर मात्रा में श्रेय, यश, पुण्य आदि सहज ही प्राप्त कर सकता है। उन्हें समझकर भी, उनका लाभ उठाने की चाह होने पर भी अधिकांश व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाते। ब्राह्मणोचित वृत्तियों के अभाव में बाहर के आकर्षण और अंदर की लिप्सा आदि से जूझ पाना उनके लिए संभव नहीं होता। इसीलिये अवसरों का लाभ उठाने की इच्छा होते हुए भी प्रयास सफल नहीं होते। ब्राह्मण वृत्ति ही वह सामर्थ्य साधकों में पैदा करती है ।। युगऋषि अपनी जीवनी मेंब्राह्मण जीवन और ऋषि कर्म' शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं :-
"अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जागते ही बहिरंग में साधु प्रवृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात् लिप्सा से जूझ सकने योग्य मनोबल का धनी। प्रलोभनों और दबावों का सामना करने में समर्थ। औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने में संतुष्टि अनुभव करने वाला साधक। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये प्रारंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक का समर्थ प्रशिक्षण मिला। वही ब्राह्मण जन्म था। माता- पिता तो एकमांस- पिण्ड को जन्म पहले ही दे चुके थे।"
मांस पिण्ड के अंदर स्थित जीवन चेतना जब समर्थ मार्गदर्शक गुरू के निर्देशन में अपने अंदर ब्राह्मण वृत्तियों को जाग्रत्, विकसित करने के लिये कमर कसकर सक्रिय हो जाती है, तभी उसका दूसरा जन्म होता है। श्रावणी पर्व इसी दिव्य पुरुषार्थ में पूरी तत्परता से प्रवृत्त होने की प्रेरणा और उसके लिये समुचित ऊर्जा- प्रवाह लेकर आता है। पर्वायोजनों के निर्धारित कर्मकाण्ड दोहराते हुए हमें अपना ध्यान इसी बिंदु पर केन्द्रित रखना चाहिये कि हमारे मन में ब्राह्मण वृत्तियाँ पहले से बेहतर स्तर पर विकसित हो सकें। युगऋषि को मिशन के प्रमुख केन्द्रों सहित गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना और युग निर्माण अभियान के विभिन्न चरणों में जो अद्भुत सफलता मिली, उसके लिये वे प्रमुख श्रेय इस ब्राह्मण वृत्ति को ही देते हैं, लिखा है :-
"परिणाम आश्चर्यजनक हुए है। अगले दिनों जो होने वाला है उन्हें अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परम्परा अपनाने में बरती गयी तत्परता है।"
इस कार्य में साधनों और समयदान के रूप मे परिजनों का जो अद्वितीय सहयोग प्राप्त हुआ, उसके पीछे वह इसी वृत्ति को, प्रामाणिकता को ही देखते हैं। लिखा है :-
"इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरान्त यह विश्वास उभरना कि यहाँ ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है।"
जन- जन का यह विश्वास अनायास ही नहीं उभर आता। जीवन के हर पक्ष में व्यक्ति को प्रामाणिकता की कसौटी पर परखा जाता है, तभी यह पावन प्रतिष्ठा मिलती है। नवयुग अवतरण के क्रम में अभी भी बड़ी संख्या में जन- जन के श्रम- साधन आदि का नियोजन किया जाना ज़रूरीहै। यह तभी संभव होगा, जब हम सब अपने अन्दर ब्राह्मण वृत्ति को क्रमश: अधिक जीवन्त और प्रामाणिक बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटे रहें। जो जिस स्तर पर है वह उससे एक क़दम आगे बढ़ने की साधना में प्रवृत्त हो। तभी ऐसे व्यक्तित्व उभरेंगे जो आने वाली बड़ीज़िम्मेदारियों को सँभाल सकेंगे।
पर्व के सन्दर्भ से
श्रावणी पर्व के विभिन्न कर्मकाण्डों के साथ जुड़ी भावनाओं को विकसित किया जाय तो युगधर्म के पालन के क्रम में आने वाली तमाम कठिनाइयाँ क्रमश: हल होती जायेंगी।
प्रायश्चित विधान :- युगऋषि से प्रभावित होकर हमने युगसाधना में प्रवृत्त होने, युगधर्म का पालन करने के संकल्प लिए। उसके निर्धारित नियमों के नियमित अनुपालन में कहाँ- कहाँ चूकें हुईं, उन्हें खोजें।
स्थूल नियमों, कर्मकाण्डों का पालन करते हुए ऋषि निर्देशों के अनुरूप भावना प्रकट करने में कहाँ कमी रह गयी, उसकी निष्पक्ष समीक्षा करें।
दोनों तरह की चूकों को सच्चे मन से स्वीकारें। उसके लिए किन्हीं व्यक्तियों या परिस्थितियों को दोष देने की जगह अपनी तत्परता की कमीआँके। बिगड़े हुए माहौल में ही हमें अपने दायित्व पूरे करने हैं। उनके अनुसार अपनी तैयारी करते रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने अविवेक या तत्परता की कमी का अनुभव करते हुए पश्चाताप का भाव लायें। गुरुसत्ता एवं आत्मदेव से प्रार्थना करें कि तमाम विसंगतियों के बावजूद हमें युगधर्म की कसौटी पर तो खरा उतरना है। इसी निमित्त प्रायश्चित्त विधान से चित्त को शुद्ध करके, ब्राह्मण वृत्तियों को जाग्रत्- जीवन्त बनाना है।
दश स्नान की शारीरिक क्रियाओं के साथ मनःसंस्थान को निर्मल एवं समर्थ बनाने के भावों में डूबकर कर्मकाण्ड करें। हेमाद्रि संकल्प भी इसी प्रायश्चित्त विधान का अंग है।
पूजन क्रम के अंतर्गत शिखा पूजन के समय यह भाव उभरे- पुष्ट हो कि हम शिखाधारी हैं। हमारे आदर्श ऊँचे- शिखर जैसे होने चाहिए। निम्नगामी व्यक्तियों और घटनाओं से हमें प्रभावित नहीं होना है।
यज्ञोपवीत पूजन के समय भाव करें कि हम मेले की भीड़ में शामिल नहीं हैं। हम मेले को अनुशासित- व्यवस्थित बनाने वाले स्काउट या सैनिक हैं। यज्ञोपवीत के यज्ञीय अनुशासनों को हमने स्वतः: स्वीकार किया है। उन अनुशासनों को पालन करने, अज्ञान- अशक्ति का निवारण करने में हमारी प्रखरता और दक्षता बढ़ती ही रहनी चाहिए।
वेद पूजन, ऋषि पूजन :- वेद पूजन के अनुकूल भाव विकसित हो तो वेददूत बनने, ज्ञानक्रान्ति को तीव्रतर गति देने की हमारी क्षमता बढ़ेगी ही। ऋषि पूजन के अनुरूप भाव पुष्ट होंगे तो महापुरुषों के यशगान से अधिक उनके अनुशासनों को जीवन में उतारने की तत्परता बढ़ जायेगी। नैतिक क्रान्ति जीवन क्रम में फूट पड़ेगी।
रक्षाबन्धन की भावना जीवन्त हो उठे तो हर युवक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो उठे। हर नारी बहन के भाव से सज्जन पुरुषार्थियों की सुरक्षा के लिए दिव्य रक्षा कवच बनने में समर्थ हो जाये।
आइये! युगऋषि की साक्षी में श्रावणी पर्व को कुछ ऐसी जीवन्तता प्रदान करें कि युगक्रान्ति के लिए तेजस्वी साधकों की संख्या और गुणवत्ता में वाञ्छित वृद्धि होती रह सके।
महापर्व- श्रावणी पर्व
श्रावणी पर्व का महत्त्व ऋषि परम्परा के अनुसार बहुत अधिक रहा है। यह पर्व द्विजत्व को विकसित और पुष्ट बनाने वाला विशिष्ट पर्व रहा है। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर दिव्य क्षमताएँ बीज रूप में होती हैं। उन्हें संतुलित साधना द्वारा विकसित करके हर व्यक्ति मानव से महामानव- देवमानव बन सकता है। नर से नारायण बनने के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ऋषिकल्प- गुरुओं के अनुशासन में उस संतुलित साधना को अपनाने के संकल्पयुक्त संस्कार को द्विजत्व का संस्कार कहा जाता है। मनुष्य उसी काया के रहते नये जन्म, दूसरे दिव्य जन्म का लाभ उठा सकता है। इस संस्कार के द्वारा ऋषि अनुग्रह और अपने साधना पुरुषार्थ के सुसंयोग से साधक अपने व्यक्तित्व में नयी सृष्टि का अनुपम लाभ प्राप्त करता है। युगऋषि ने पर्वों के महत्त्व के क्रम में यह लिखा है कि श्रावणी पर्व का सम्बन्ध उस समय से है, जब परब्रह्म- परमात्मा ने 'एकोऽहम बहुस्याम' का संकल्प किया। परब्रह्म का संकल्प होते ही उनकी अभिन्न चेतन शक्ति- आद्यशक्ति ने तत्काल सृष्टि को स्वरूप प्रदान कर दिया। इस नाते श्रावणी पर्व के साथ आदिशक्ति- चिद्शक्ति का सृजनशील प्रवाह जुड़ा रहता है। साधक के अन्दर कोई सत्संकल्प आकार लेता है तो वह शक्ति उसे साकार करने के लिए अपना समर्थ सहयोग अनायास ही प्रदान करने लगती है। साधक इस दिव्य ऊर्जा प्रवाह का लाभ उठाकर अपने जीवन में एक नयी सृष्टि करने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए इसे द्विजत्व के संकल्प को परिष्कृत और पुष्ट बनाकर जीवन लक्ष्य तक पहुँचने के पुण्य पर्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।
संकल्प कैसा : प्रश्न है कि जब प्रकृति का प्रवाह श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने की दिव्य ऊर्जा के साथ अवतरित हो रहा हो तो कैसा संकल्प किया जाय? चिन्तन करने पर सहज ही यह उत्तर उभरेगा कि ऐसे मौके पर सोने जैसा खरा और बड़ा संकल्प लिया जाय। इसीलिए ऋषियों ने श्रावणी पर्व के संकल्प को हेमाद्रि संकल्प नाम दिया। हेम शुद्ध सोने को कहते हैं और अद्रि पर्वत का पर्याय है। अर्थात् ऐसे महत्त्वपूर्ण पर्व पर शुद्ध सोने के पर्वत जैसा संकल्प करना चाहिए। जीवन को द्विजत्व के मार्ग से नर से नारायण के स्तर पर ले जाने वाले संकल्प को ही वास्तव में हेमाद्रि संकल्प कहा जा सकता है।
श्रावणी पर्व पर हेमाद्रि संकल्प के साथ जुड़े अन्य कर्मकाण्ड दश स्नान, ऋषि पूजन, वेद पूजन आदि भी द्विजत्व की साधना को सिद्ध करने के सूत्रों को हृदयंगम कराने वाले हैं। आवश्यकता है उन्हें यंत्रवत पूरा न करके उनके अनुरूप भावनाओं को जाग्रत् और सक्रिय किया जाय। इसी आधार पर विकसित की गयी साधना वे परिणाम उत्पन्न करती है, जिन्हें ऋषियों- मनीषियों ने अद्भुत- अनुपम कहा है।
ऋषियुग्म के अनुभव अपनी जीवनी 'हमारी वसीयत और विरासत' में युगऋषि ने साधना के कर्मकाण्डों से अधिक महत्त्व उनसे सम्बद्ध भावनाओं को देने की बात कही है। अपनी सफल साधना का मर्म समझाते हुए वे लिखते हैं-
"हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। निर्धारित जप संख्या को पूरा करने का अनुशासन कठोरतापूर्वक पाला गया। आपात स्थिति में कोई कमी रह गयी तो उसे अगले दिनों में पूरा कर लिया गया। इसी के साथ उस अवधि में भावनाओं से ओतप्रोत रहने कीमनःस्थिति बनाये रहने का अभ्यास किया गया है और वह सफल भी होता रहा है। समर्पण, एकता, एकात्मता, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ में कल्पना के रूप में किया गया था। पीछे वह मान्यता बन गयी और अन्त में अनुभूति प्रतीत होने लगी।"
संकल्पित जप- कर्मकाण्ड आदि का पालन पूरी निष्ठा से करने के साथ ही साथ इष्ट के अनुकूल भावनाओं को जीवन्त और सतत बनाये रखने के प्रयास भी पूरी तत्परता से करने के संकल्पित प्रयासों ने उनकी साधना को सिद्धि तक पहुँचाया। इस प्रयास में भी कई साधक बीच में ही उलझकर रह जाते हैं। कल्पना को ही उपलब्धि मानकर आत्मसम्मोहन की स्थिति में ही जीते रहते हैं, मान्यता और अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच पाते। इस सम्मोहन से उबरने के लिए बहुत विवेकपूर्वक ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण- परीक्षण भी करना पड़ता है। गुरुवर ने इस सम्बन्ध में लिखा है :-
'गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी। यह मात्र कल्पना तो नहीं है, इसके लिए बार- बार कठोर आत्म निरीक्षण किया जाता रहा। देखा गया कि आदर्श जीवन के प्रति- समष्टि के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं? आदर्शों के लिए प्रलोभनों और दबावों से इन्कार करने की स्थिति है या नहीं? समय- समय पर घटनाओं से जोड़कर भी परख की गयी और पाया गया कि भावना परिपक्व हो गयी है। ... मान्यता का गुण- कर्म में परिवर्तन होना, यही तो उपासनात्मक धारणा की परख है।'
बालक श्रीराम को उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय यह बात समझाई गयी थी कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। उन्होंने अपने मन- अन्तःकरण को ब्राह्मण के स्तर का बनाने की भावभरी तप साधना की। उन्हें उसका भरपूर लाभ मिला। उन्हीं के चरण- चिह्नों पर चलते हुए हम सबकों 'ब्राह्मणत्व संवर्धन' के पर्व श्रावणी पर अपने मन को ब्राह्मण के साँचे में ढालने के प्रयास किये जाने चाहिये। अपने साधना पुरुषार्थके लाभ उन्हीं की तरह कमाने की भूमिका बनानी चाहिये।
ब्राह्मणत्व का महत्त्व
समय- समय पर ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर आते हैं, जिनका लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति प्रचुर मात्रा में श्रेय, यश, पुण्य आदि सहज ही प्राप्त कर सकता है। उन्हें समझकर भी, उनका लाभ उठाने की चाह होने पर भी अधिकांश व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाते। ब्राह्मणोचित वृत्तियों के अभाव में बाहर के आकर्षण और अंदर की लिप्सा आदि से जूझ पाना उनके लिए संभव नहीं होता। इसीलिये अवसरों का लाभ उठाने की इच्छा होते हुए भी प्रयास सफल नहीं होते। ब्राह्मण वृत्ति ही वह सामर्थ्य साधकों में पैदा करती है ।। युगऋषि अपनी जीवनी मेंब्राह्मण जीवन और ऋषि कर्म' शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं :-
"अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जागते ही बहिरंग में साधु प्रवृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात् लिप्सा से जूझ सकने योग्य मनोबल का धनी। प्रलोभनों और दबावों का सामना करने में समर्थ। औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने में संतुष्टि अनुभव करने वाला साधक। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये प्रारंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक का समर्थ प्रशिक्षण मिला। वही ब्राह्मण जन्म था। माता- पिता तो एकमांस- पिण्ड को जन्म पहले ही दे चुके थे।"
मांस पिण्ड के अंदर स्थित जीवन चेतना जब समर्थ मार्गदर्शक गुरू के निर्देशन में अपने अंदर ब्राह्मण वृत्तियों को जाग्रत्, विकसित करने के लिये कमर कसकर सक्रिय हो जाती है, तभी उसका दूसरा जन्म होता है। श्रावणी पर्व इसी दिव्य पुरुषार्थ में पूरी तत्परता से प्रवृत्त होने की प्रेरणा और उसके लिये समुचित ऊर्जा- प्रवाह लेकर आता है। पर्वायोजनों के निर्धारित कर्मकाण्ड दोहराते हुए हमें अपना ध्यान इसी बिंदु पर केन्द्रित रखना चाहिये कि हमारे मन में ब्राह्मण वृत्तियाँ पहले से बेहतर स्तर पर विकसित हो सकें। युगऋषि को मिशन के प्रमुख केन्द्रों सहित गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना और युग निर्माण अभियान के विभिन्न चरणों में जो अद्भुत सफलता मिली, उसके लिये वे प्रमुख श्रेय इस ब्राह्मण वृत्ति को ही देते हैं, लिखा है :-
"परिणाम आश्चर्यजनक हुए है। अगले दिनों जो होने वाला है उन्हें अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परम्परा अपनाने में बरती गयी तत्परता है।"
इस कार्य में साधनों और समयदान के रूप मे परिजनों का जो अद्वितीय सहयोग प्राप्त हुआ, उसके पीछे वह इसी वृत्ति को, प्रामाणिकता को ही देखते हैं। लिखा है :-
"इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरान्त यह विश्वास उभरना कि यहाँ ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है।"
जन- जन का यह विश्वास अनायास ही नहीं उभर आता। जीवन के हर पक्ष में व्यक्ति को प्रामाणिकता की कसौटी पर परखा जाता है, तभी यह पावन प्रतिष्ठा मिलती है। नवयुग अवतरण के क्रम में अभी भी बड़ी संख्या में जन- जन के श्रम- साधन आदि का नियोजन किया जाना ज़रूरीहै। यह तभी संभव होगा, जब हम सब अपने अन्दर ब्राह्मण वृत्ति को क्रमश: अधिक जीवन्त और प्रामाणिक बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटे रहें। जो जिस स्तर पर है वह उससे एक क़दम आगे बढ़ने की साधना में प्रवृत्त हो। तभी ऐसे व्यक्तित्व उभरेंगे जो आने वाली बड़ीज़िम्मेदारियों को सँभाल सकेंगे।
पर्व के सन्दर्भ से
श्रावणी पर्व के विभिन्न कर्मकाण्डों के साथ जुड़ी भावनाओं को विकसित किया जाय तो युगधर्म के पालन के क्रम में आने वाली तमाम कठिनाइयाँ क्रमश: हल होती जायेंगी।
प्रायश्चित विधान :- युगऋषि से प्रभावित होकर हमने युगसाधना में प्रवृत्त होने, युगधर्म का पालन करने के संकल्प लिए। उसके निर्धारित नियमों के नियमित अनुपालन में कहाँ- कहाँ चूकें हुईं, उन्हें खोजें।
स्थूल नियमों, कर्मकाण्डों का पालन करते हुए ऋषि निर्देशों के अनुरूप भावना प्रकट करने में कहाँ कमी रह गयी, उसकी निष्पक्ष समीक्षा करें।
दोनों तरह की चूकों को सच्चे मन से स्वीकारें। उसके लिए किन्हीं व्यक्तियों या परिस्थितियों को दोष देने की जगह अपनी तत्परता की कमीआँके। बिगड़े हुए माहौल में ही हमें अपने दायित्व पूरे करने हैं। उनके अनुसार अपनी तैयारी करते रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने अविवेक या तत्परता की कमी का अनुभव करते हुए पश्चाताप का भाव लायें। गुरुसत्ता एवं आत्मदेव से प्रार्थना करें कि तमाम विसंगतियों के बावजूद हमें युगधर्म की कसौटी पर तो खरा उतरना है। इसी निमित्त प्रायश्चित्त विधान से चित्त को शुद्ध करके, ब्राह्मण वृत्तियों को जाग्रत्- जीवन्त बनाना है।
दश स्नान की शारीरिक क्रियाओं के साथ मनःसंस्थान को निर्मल एवं समर्थ बनाने के भावों में डूबकर कर्मकाण्ड करें। हेमाद्रि संकल्प भी इसी प्रायश्चित्त विधान का अंग है।
पूजन क्रम के अंतर्गत शिखा पूजन के समय यह भाव उभरे- पुष्ट हो कि हम शिखाधारी हैं। हमारे आदर्श ऊँचे- शिखर जैसे होने चाहिए। निम्नगामी व्यक्तियों और घटनाओं से हमें प्रभावित नहीं होना है।
यज्ञोपवीत पूजन के समय भाव करें कि हम मेले की भीड़ में शामिल नहीं हैं। हम मेले को अनुशासित- व्यवस्थित बनाने वाले स्काउट या सैनिक हैं। यज्ञोपवीत के यज्ञीय अनुशासनों को हमने स्वतः: स्वीकार किया है। उन अनुशासनों को पालन करने, अज्ञान- अशक्ति का निवारण करने में हमारी प्रखरता और दक्षता बढ़ती ही रहनी चाहिए।
वेद पूजन, ऋषि पूजन :- वेद पूजन के अनुकूल भाव विकसित हो तो वेददूत बनने, ज्ञानक्रान्ति को तीव्रतर गति देने की हमारी क्षमता बढ़ेगी ही। ऋषि पूजन के अनुरूप भाव पुष्ट होंगे तो महापुरुषों के यशगान से अधिक उनके अनुशासनों को जीवन में उतारने की तत्परता बढ़ जायेगी। नैतिक क्रान्ति जीवन क्रम में फूट पड़ेगी।
रक्षाबन्धन की भावना जीवन्त हो उठे तो हर युवक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो उठे। हर नारी बहन के भाव से सज्जन पुरुषार्थियों की सुरक्षा के लिए दिव्य रक्षा कवच बनने में समर्थ हो जाये।
आइये! युगऋषि की साक्षी में श्रावणी पर्व को कुछ ऐसी जीवन्तता प्रदान करें कि युगक्रान्ति के लिए तेजस्वी साधकों की संख्या और गुणवत्ता में वाञ्छित वृद्धि होती रह सके।